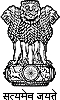हमें सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है
सामाजिक सुरक्षा न केवल अपने उपभोक्ताओं को बल्कि उसके संपूर्ण परिवार को भी वित्तीय एवं स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ प्रदान करती है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का निर्माण परिवार के कमाने वाले सदस्य के सेवानिवृत होने पर या उसकी मृत्यु हो जाने पर या किसी अक्षमता का शिकार हो जाने की स्थिति में दीर्घकालीन सहायता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। इस प्रकार सामाजिक सुरक्षा की मुख्य विशेषता यह है कि यह प्रदाता के रूप में काम करती है- यह बीमा और सहायता के जरिए लोगों को उनके भविष्य की योजना बनाने में मदद करती है। बहरहाल, सामाजिक सुरक्षा योजना की सफलता के लिए कर्मचारियों और नियोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक होती है।
बतौर कर्मचारी आप अपने और अपने परिवर की सामाजिक सुरक्षा के स्रोत हैं। बतौर नियोक्ता आप अपने सभी कर्मचारियों को पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के जिम्मेदार हैं।
सामाजिक सुरक्षा पर पृष्ठभूमि जानकारी
भारत में हमेशा से संयुक्त परिवार की व्यवस्था रही है जो अपने सभी सदस्यों की सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति करती रही है जिसके लिए जमीन जैसी भौतिक संपदा तक उसकी (संयुक्त परिवार की) पहुंच होती है या उसपर उसका स्वामित्व होता है। अपनी सांस्कृतिक परंपरा को बनाए रखने के लिए परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के प्रति साझी जिम्मेदारी की भावना से भरे होते हैं। जिस सीमा तक परिवार के पास संसाधन की उपलब्धता रहती है उस सीमा तक परिवार के बुजुर्गों और बीमारों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति होती है।
यद्यपि, बढ़ते हुए उत्प्रवास, शहरीकरण और जनांकिकीय परिवर्तनों के कारण बड़े आकार वाले संयुक्त परिवारों की संख्या में कमी आती गई। यहीं पर सामाजिक सुरक्षा की औपचारिक व्यवस्था महत्वपूर्ण हो जाती है। बहरहाल, सामाजिक सुरक्षा के दायरे को विस्तृत करने में सूचना और जागरुकता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। भारत में सामाजिक सुरक्षा लाभ आवश्यकता-आधारित है, यानि सामाजिक सहायता के घटक सार्वजनिक रूप से प्रबंधित योजनाओं में अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। भारतीय संदर्भ में, सामाजिक सुरक्षा एक समग्र अधिगम है जिसका निर्माण व्यक्ति को आर्थिक अभाव से बचाने और व्यक्ति के खुद के लिए तथा उसके आश्रितों के लिए, उन्हें आर्थिक अनिश्चयता की स्थिति से बचाने हेतु एक न्यूनतम आय की सुनिश्चितता के लिए किया गया है। अपने कर्मचारियों को सुरक्षा और सहायता करने के लिए उचित व्यवस्था के निर्माण की जिम्मेदारी प्राथमिक रूप से राज्य की होती है। सामाजिक सुरक्षा को निरंतर विकास प्रक्रिया के एक अंग के रूप में देखा जाता है। वैश्वीकरण और उसके कारण होने वाले संरचनात्मक और तकनीकी परिवर्तनों से उपजी चुनौतियों से निबटने के लिए यह अधिक सकारात्मक रवैये के निर्माण में सहायता करती है।
भारत में कार्यबल
संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों को ध्यान में रखकर भारत में समस्याओं के आयाम और उनकी जटिलताओं को अधिक सही तरीके से समझा जा सकता है। वर्ष 2004-005 के एनएसएसओ सर्वेक्षण ने इन दो क्षेत्रों की व्यापक भिन्नता को इंगित किया। जहां वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार कुल कार्यबल 31 करोड़ 40 लाख था और संगठित क्षेत्र ने इसमें केवल 2 करोड़ 70 लाख का योगदान दिया, वहीं वर्ष 2004-05 में नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन (एनएसएसओ) द्वारा संचालित सर्वेक्षण के अनुसार कार्यबल की कुल संख्या 45 करोड़ 90 लाख थी, जिसका लगभग 43 करोड़ 3 लाख (लगभग 94%) असंगठित क्षेत्र में और 2 करोड़ 60 लाख कार्यबल संगठित क्षेत्र में शामिल थे। संगठित क्षेत्र को पहले से ही सामाजिक सुरक्षा कानूनों के तहत शामिल किया जा चुका था, जैसे कि कर्मचारी भविष्य-निधि कोष तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 व कर्मचारी राजकीय बीमा अधिनियम, 1948 इत्यादि। सरकार ने असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी असंगठित कामगार सुरक्षा अधिनियम का प्रावधान किया। इस प्रकार इन तथ्यों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि असंगठित क्षेत्र के मुकाबले संगठित क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि रही।
संगठित और असंगठित क्षेत्र
संगठित क्षेत्र में मुख्य रूप से वे संस्थाएं हैं जो कारखाना अधिनियम, 1948, राज्य सरकारों के दुकान एवं व्यावसायिक संस्थान अधिनियम, औद्योगिक कर्मचारी स्थायी आदेश अधिनियम, 1946 आदि के तहत आती हैं। इस क्षेत्र के पास पहले से एक ढांचा है जिसके जरिए इन अधिनियमों के तहत कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्राप्त हो जाते हैं।
दूसरी ओर असंगठित क्षेत्र में श्रम कानूनों का अभाव होता है, कार्य की प्रकृति मौसमी और अस्थायी होती है, कामगारों का अत्यधिक संचलन होता है, परिचालन बिखरे हुए तरीके से होता है, नियमित श्रमिकों की अल्पकालीन पुनर्नियुक्ति होती है, सांगठनिक संबल का अभाव होता, मोलभाव करने की निम्न क्षमता होती है आदि..आदि, जिनके कारण इस क्षेत्र के कामगार सामाजिक-आर्थिक कठिनाइयों से घिरे होते हैं। असंगठित क्षेत्र में काम की प्रकृति अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग होती है, साथ ही ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में भी इसकी प्रकृति अलग-अलग होती है, जिसमें शामिल हैं दूर-दराज के ग्रामीण इलाके और सभी-कभी सबसे असंवेदनशील शहरी क्षेत्र। ग्रामीण इलाकों में इसके तहत भूमिहीन खेतिहर मजदूर, छोटे और सीमांत किसान, बटाईदार, पशुपालन और मत्स्य पालन करने वाले, बागवानी करने वाले, मधुमक्खी पालक, ताड़ी उतारने वाले, जंगल में काम करने वाले, ग्रामीण दस्तकार आदि आते हैं, जबकि शहरी इलाकों में इसमें निर्माण क्षेत्र के मजदूर, बढ़ई, व्यापारी, परिवहन संचार आदि में लगे लोग आते हैं और साथ ही इनमें सड़क पर सामान बेचने वाले, रेहड़ी लगाने वाले, फेरी वाले, सिर पर बोझा ढोने वाले, मोची, टिन का काम करने वाले, कपड़ा तैयार करने वाले लोग भी आते हैं।
सामाजिक सुरक्षा कानून का सारांश
भारत में लागू कुछ मुख्य सामाजिक सुरक्षा कानून इस प्रकार हैं:
- कर्मचारियों का राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (ईएसआई एक्ट) जिसके दायरे में ऐसे कारखाने और संस्थाएं आते हैं जिनमें 10 या अधिक श्रमिक काम करते हों और यह अधिनियम कामगारों और उनके परिवारों के लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ बीमार होने और बच्चे के जन्म की स्थिति में नकद लाभ तथा मृत्यु या शारीरिक अक्षमता की स्थिति में मासिक भुगतान का प्रावधान करता है।
- कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (ईपीडीएंडएमपी एक्ट) जो ऐसे विशेष अनुसूचित कारखानों और संस्थानों पर लागू होते हैं जिनमें 20 या अधिक कर्मचारी काम करते हैं और यह अधिनियम भविष्य निधि पर टर्मिनल लाभ, सुपरएन्युएशन पेंशन, और सेवा के दौरान मृत्यु होने पर परिवार पेंशन का प्रावधान करता है। कोयले की खदानों और चाय बागानों के कामगारों के लिए इन्हीं प्रकारों के लाभ हेतु अलग से कानून हैं।
- कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 (डब्ल्यूसी एक्ट), जो काम के दौरान घायल होने के कारण मृत्यु या शारीरिक अक्षमता की स्थिति में कामगार या उसके परिवार को क्षतिपूर्ति के भुगतान का प्रावधान करता है।
- मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 (एम.बी. एक्ट), जो बच्चे के जन्म की स्थिति में 12 सप्ताह के सवैतनिक अवकाश और मातृत्व संबंधी अन्य मामलों में भुगतान सहित अवकाश का प्रावधान करता है।
- ग्रैच्युइटी भुगतान अधिनियम, 1972 (पी.जी. एक्ट), जिसमें न्यूनतम 10 कामगारों वाले संस्थान में पांच साल या अधिक काम किए हुए कर्मचारियों को हर साल 15 साल दिनों का वेतन देने का प्रावधान है।
कोयला खदानों और असम के चाय बागानों के श्रमिकों तथा सागरकर्मियों के लिए पृथक भविष्य निधि कोष अधिनियम।
नई पहल-
द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में सामाजिक सुरक्षा पर विभिन्न केन्द्रीय अधिनियमों का परीक्षण किया जा रहा है। ईएसआईसी अधिनियम में आवश्यक सुधार किए गए हैं, जबकि ईपीएफ तथा एमपी ऐक्ट की विशद् समीक्षा अभी जारी है। मातृत्व लाभ योजना और कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम के लिए प्राप्त संशोधन के प्रस्तावों पर परामर्श की प्रकिया जारी है।
ईपीएफओ तथा ईएसआईसी की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के परिचालन में अभिनव उपायों के प्रस्ताव हैं। इन प्रस्तावों में शामिल हैं लोचशील लाभ योजनाएं जिन्हें जनसंख्या के विभिन्न हिस्सों की अपनी-अपनी जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है।
ईपीएफओ तथा ईएसआईसी की क्रियाविधि में वर्तमान उपायों का सारांश
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रोफाइल को व्यापक पहुंच और ग्राहक संतुष्टि को ध्यान में रखकर परिवर्तित किया गया है।
ईपीएफओ के दायरे में सपूर्ण देश आता है जिसके तहत 393824 संस्थान आते हैं। वर्तमान में, 11.80 करोड़ ईपीएफ सदस्य और उनके परिवारों को ईपीएफओ द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत लाभ मिल रहा है। ईपीएफ योजना 1952, ईडीएलआई योजना, 1976 तथा कर्माचारी पेंशन योजना 1995 के तहत संयुक्त धनराशि 31-3-2014 को लगभग 5,36,993 करोड़ रुपए की है। बीते सालों में, ग्राहकों को दी जाने वाली सेवा का परिमाण और साथ ही किए जाने वाले निवेश आदि, जो ईपीएफओ द्वारा किए हैं, कई गुना बढ़ गए हैं। ग्राहकों और कर्मचारियों को बेहतर सेवा देने के उद्देश्य से संगठन के परियोजना री-इनवेंटिंग ईपीएफ, इंडिया का शुभारंभ जून, 2001 में किया है। इस परियोजन का मुख्य उद्देश्य है ग्राहकों को उत्कृष्ट और प्रभावी सेवा प्रदान करना, कर्मचारियों को उनकी शिकायतों के अवसर में कमी लाकर मदद करना और संगठनों को सभी क्षेत्रों में ज्यामितीय उन्नति करने में सहायता करना। इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण भाग है ईपीएफ ग्राहकों को यूनिक आडेंटिफिकेशन नम्बर- सामाजिक सुरक्षा संख्या उपलब्ध कराना, नियोक्ताओं तथा बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग को बिजनेस नम्बर उपलब्ध कराना।
क्रियान्वयन की रणनीति विकसित की गई है सामाजिक सुरक्षा संख्या का आवंटन प्रभावी आंकड़ा संग्रह के लघु चरणों में संपन्न किए जाने वाले संपूर्ण क्रियाकलाप के साथ आरंभ किया गया है। एसएसएन के आवंटन के लिए जिन मानदंडों पर विचार किया जा रहा है उनमें शामिल हैं विशिष्टता का केन्द्रीकृत नियंत्रण जिससे आवंटन के दौरान न्यूनतम मैनुअल हस्तक्षेप सुनिश्चित किया गया है और 100% विशिष्टता के सटीकता स्तर तय किए गए हैं। संक्षेप में सामाजिक सुरक्षा संख्या प्रवासी मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने और ईपीएफओ के डेटाबेस को कामगारों के बीच उच्च कार्य संचलन के मौजूदा रुझान के लिए अपनाए जाने योग्य होगा।
सामाजिक सुरक्षा लोगों और समाज की भलाई के लिए आवश्यक है। यह मौलिक मानवाधिकार है और इसका क्रियान्वयन देश के विभिन्न विकास लक्ष्यों को पूरा करने में अपनी भूमिका निभाएगा। सामाजिक सुरक्षा उपाय के दूरगामी लाभ नागरिकों में गर्व और आत्मसम्मान की भावना के रूप में होंगे। ऐसे उपाय कार्य परिस्थितियों के अंतर्गत स्वास्थ्य और जीवन के अन्य खतरों के विरुद्ध न्यूनतम स्तर की सुरक्षा प्रदान करते हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, मातृत्व सुविधा और वृद्धावस्था पेंशन उपलब्ध करने में सामाजिक सुरक्षा के लिए यह उत्तरोत्तर मानक की भूमिका निभाएगा।
संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के साधन के माध्यम से प्रदान की जाती है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ)
जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर ईपीएफओ का प्रसार पूरे देश भर में हो चुका है, जिसके तहत 31 मार्च 2014 तक 7.98 लाख प्रतिष्ठानों को शामिल किया जा चुका है। इसके अलावा लगभग 11.80 करोड़ ईपीएफ सदस्य तथा उनके परिवारों को 31 मार्च 2014 तक ईपीएफओ द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का फायदा पहुंचाया जा चुका है। 31 मार्च 2014 तक कुल निवेश राशि 0 7,30,393/ करोड़ (0 5,36,993/- करोड़, गैर-छूट प्राप्त कोष तथा 0 1,93,400/- करोड़ छूट-प्राप्त कोष शामिल है) रहा। बीते सालों में, ईपीएफओ द्वारा ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं के परिमाण और निवेश में कई गुना इजाफा हुआ है। ईपीएफओ ने सदस्यों तक बेहतर तरीके से, कुशलतापूर्वक समुन्नत सेवा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया के स्वचालीकरण हेतु अपने प्रयासों को केन्द्रित किया है। इस दिशा में किए गए कार्य इस प्रकार हैं:-
- ईपीएफओ के सभी 120 कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2012-2013 से सांविधिक ईपीएफ रिटर्न (ईसीआर – इलेक्ट्रॉनिक चालान सह रिटर्न) को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा कराने की सुविधा का आरंभ किया गया है। यह विप्रेषण के साथ रिटर्न फाइल करने का एक अनिवार्य तरीका है, जिसने नियोक्ताओं को किसी भी स्थान से हर महीने ऑनलाइन तरीके से एक ही (हर महीने 4 और दो वार्षिक रिटर्न की बजाए) रिटर्न फाइल करने की सुविधा प्रदान की।
- कर्मचारी अपने ईपीएफ बकाए का प्रेषण इलेक्ट्रॉनिक विधि से कर सकते हैं, बशर्ते उनका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंक खाता हो।
- जिन कर्मचारियों का एसबीआई में कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंक खाता नहीं है उन्हें चेक/डीडी के जरिए ईपीएफ बकाए का भुगतान करना होगा।
- उपरोक्त रिटर्न के इलेक्ट्रॉनिक विधि से प्राप्त होने के बाद कनफर्म हो जाने पर सदस्य का खाता मासिक रूप से अद्यतन किया जाता है। इसलिए अब सदस्यों को वित्तीय वर्ष के अंत तक उनके पीएफ खाते में मौजूद शेष राशि जानने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी होती।
- संस्थापन अपने कर्मचारियों के वार्षिक पीएफ अकाउंट स्प्लिप्स को देख सकता है और प्रिंट कर सकता है।
- हर कर्मचारी को मेम्बर पासबुक के रूप में उसके ईपीएफ खाते के विवरण को ऑनलाइन रजिस्टर करने और उसे देखने की सुविधा प्रदान की गई है। इस पासबुक में क्रेडिट तथा निकासी के माहवार विवरण होते हैं, जबकि इससे पहले एफ-23 में एक पंक्ति का वार्षिक सारांश दिया जाता था।
- नियोक्ताओं को ईपीएफ के सांविधिक प्रावधानों का पालन करने और आवश्यक रिटर्न फाइल करने में सुविधा हो इसके लिए एक ई-रिटर्न टूल उपलब्ध कराया गया है।
- www.epfindia.gov.in पर "Know Your PF Balance" (नो योर पीएफ बैलेस) लिंक के माध्यम से अपने पीएफ बैलेंस को अपने मोबाइल फोन पर भी प्राप्त कर सकते हैं।
- सदस्य अपने दावों और भुगतानों की स्थिति को ऑनलाइन "Know Your Claim Status" (नो योर क्लेम स्टेटस) लिंक के माध्यम से ट्रैक कर सकते हैं और इसके लिए एसएमएस प्राप्त कर सकते हैं।
- ईपीएफ राशि एनईएफटी के जरिए इलेक्ट्रॉनिक विधि से लाभार्थी के बैंक खाते में प्रेषित हो जाता है। इससे दावों की पुष्टि के बाद उनके खातों में शीघ्रतापूर्वक राशि जमा की जाती है।
- ऑनलाइन ट्रांसफर क्लेम पोर्टल- ‘ओटीसीपी’ की शुरुआत के बाद ट्रांसफर क्लेम ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गई। इससे विभिन्न प्रतिष्ठानों में अपनी नौकरी के दौरान सदस्यों को शीघ्रतापूर्वक राशि हस्तांतरण की जाती है। इस सुविधा ने पहली बार नियोक्ता के डिजिटल हस्ताक्षर के साथ क्लेम फाइलिंग को सुगम बनाया है।
- छूट-प्राप्त प्रतिष्ठानों के लिए परिशिष्ट ए में दिए मासिक रिटर्न को ऑनलाइन उपलब्ध कर दिया गया है। इस प्रकार छूट-प्राप्त प्रतिष्ठानों के रोजगार, योगदान तथा निवेश विवरण डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध हो जाते हैं।
- उन ईपीएफ सदस्यों के लिए जो ऐसे देश में जाते हैं जिनका भारत के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौता किया होता है, भारत में उनके पीएफ विप्रेषण को जारी रखने के लिए कवरेज सर्टिफिकेट के निर्माण के लिए एक केंद्रीकृत सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है।
- संगठन ने भारत भर में कानूनी मामले के अनुपालन तथा निगरानी के लिए आंतरिक सॉफ्टवेयर भी चालू किया है, जिसे इसके डैशबोर्ड के जरिए मॉनिटर किया जा सकता है।
ईपीएफ और एमपी एक्ट, 1952 में एक समग्र सुधार का प्रस्ताव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में परीक्षणाधीन है और लाभार्थियों के लाभ हेतु इसमें सुधार के लिए ईपीएफओ के साथ परामर्श के अधीन है। वर्ष 2011-12 के दौरान विशेष जोर वार्षिक खाता पर्ची जारी करने पर दिया गया। 13.57 करोड़ वार्षिक खातों को इस साल अद्यतन किया गया जबकि वर्ष 2012-13 में यह आंकड़ा 12.91 करोड़ था। वर्ष 2013-14 के वार्षिक खातों का 30 सितंबर 2014 तक भुगतान दिए जाने की संभावना है। 2013-14 के दौरान 123.34 लाख ईपीएफ दावों का निबटारा किया गया और यह आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में 10.71 प्रतिशत अधिक रहा। 43.63 लाख से अधिक पेंशन धारकों को ईपीएफओ द्वारा मासिक पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी)
कर्मचारी राज्य बीमा योजना आवश्यकता आधारित सामाजिक सुरक्षा लाभ संगठित क्षेत्र के बीमाकृत कामागारों को उपलब्ध कराती है। ईपीएफओ के मामले में, ईएसआईसी ने विभिन्न समूहों की जरूरतों के लिए विभिन्न प्रकार की लाभ योजनाएं तैयार करने की महती जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। कर्मचारी राजकीय बीमा अधिनियम 1948, ऐसे कारखानों तथा प्रतिष्ठानों पर लागू होते हैं, जिनमें कम से कम 10 व्यक्ति काम करते हों, जैसे कि रोड मोटर ट्रांसपोर्ट उपक्रम, होटल, रेस्त्रां, सिनेमाघर, समाचारपत्र प्रतिष्ठान, दुकान, शिक्षा तथा मेडिकल संस्थान। हालांकि 8 राज्यों में इसके कवरेज की न्यूनतम सीमा अभी भी 20 बनी हुई है। प्रति माह रु.15,000 वेतन पाने वाले कर्मचारियों को इस अधिनियम में शामिल किया गया है, जबकि स्थायी विकलांगता के शिकार कर्मचारियों के लिए वेतन सीमा रु. 25,000 प्रति माह है। वर्तमान में इस योजना के तहत लगभग 1.86 करोड़ बीमित व्यक्तियों को शामिल किया जा रहा है, जिनमें 30 राज्यों/कें.शा. प्र के 810 केंद्र शामिल हैं। मेडिकल सेवा प्राप्त करने वाले कुल लाभार्थियों की संख्या लगभग 7.21 करोड़ है, जिनमें आईपी के परिवार वाले भी शामिल हैं।
कर्मचारी राजकीय बीमा योजना बीमित व्यक्तियों तथा उनके परिवार वालों और उनके आश्रितों को मेडिकल अटेंडेस, इलाज, दवा तथा इंजेक्शनों, विशेषीकृत परामर्श तथा अस्पताल में भर्ती के रूप में व्यापक मेडिकल सेवा प्रदान करती है। ईएसआई योजना बीमित व्यक्तियों को निम्नांकित लाभ प्रदान करती है:
- मेडिकल लाभ: यह योजना आईपी अथा उनके परिवार वालों को पूर्ण तथा व्यापक मेडिकल उपचार प्रदान करती है, जिसमें अस्पताल में भर्ती, रेफरल इलाज तथा कृत्रिम पैरों-हाथों, कृत्रिम दांत इत्यादि शामिल हैं। यह लाभ व्यक्ति को उसी समय से उपलब्ध हो जाती है, जब वह बीमा योग्य रोजगार में शामिल होता है और उसके बाद यह 6 महीनों की अवधि तक कम से कम 78 दिनों का कार्य योगदान देने की शर्त पूरा करने पर आगे भी चालू रहता है।
- रुग्णता लाभ: योजना के तहत आईपी को एक वर्ष में 91 दिनों का रुग्णता लाभ मिलता है, जो उसके वेतन का 70% तक होता है। पुरानी बीमारी की स्थिति में यह 2 वर्ष तक लागू होता है और ऐसी स्थिति में वेतन का 80% लाभ प्राप्त होता है। इस लाभ के लिए आईपी को 6 महीने में कम से कम 78 दिनों के कार्य योगदान की शर्त पूरी करनी होती है।
- मातृत्व लाभ: इस योजना के तहत मातृत्व लाभ प्रदान किया जाता है, जो 12 हफ्तों के वेतन के समतुल्य होता है और साथ ही यदि गर्भावस्था या शिशु जन्म इत्यादि के कारण कोई रोग पैदा होता है, तो ऐसे में अतिरिक्त 1 महीने का वेतन शामिल किया जाता है। इस लाभ के लिए बीमित महिला को दो योगदान अवधियों में 70 दिनों का योगदान देना होता है।
- विकलांगता लाभ: काम के दौरान जख्मी होने कारण, जिसमें पेशागत रोग भी शमिल हैं, यदि विकलांगता पैदा होती है, तो ऐसी स्थिति में आईपी को इलाज के दौरान अनुपस्थित होने पर उस अवधि के वेतन का 90% लाभ प्राप्त होता है। इस लाभ के लिए कोई योगदान शर्त नहीं है। इलाज खत्म हो जाने के बाद यदि कोई स्थायी विकलांगता पाई जाती है तो एक मेडिकल बोर्ड पूर्ण दर के एक प्रतिशत के रूप में दैनिक क्षतिपूर्ति राशि का निर्णय लेगा।
- आश्रित लाभ: काम के दौरान जख्मी होने के कारण यदि व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उसके परिवार को उसके कुल वेतन के 90% के रूप में आश्रित लाभ प्राप्त होता है।
- दाहकर्म व्यय: आईपी की मृत्यु की स्थिति में रु. 10,000/- की राशि प्रदान की जाती है, ताकि मृतक का दाहकर्म संपन्न किया जा सके।
- राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना ( बेरोजगारी भत्ता योजना): राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना की शुरुआत 01.04.2005 को की गई। इस योजना के तहत उन कर्मचारियों को शामिल किया जाता है, जिन्हें कारखानों/प्रतिष्ठानों, छंटनी या स्थायी अवैधता के कारण अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों को एक वर्ष के वेतन के 50% का समतुल्य भत्ता मिलता है।
किसी बीमित व्यक्ति, उसके परिवार और उसके आश्रितों को बीमायोग्य रोजगार में प्रवेश के दिन से ही मेडिकल लाभ प्राप्त करने का अधिकार होता है। अनेक प्रकार की मेडिकल सेवाएं प्रोत्साहक, सुरक्षात्मक, उपचारात्मक और पुनर्वास संबंधी सेवाओं पर कवर प्रदान की जाती है जिसमें शामिल है आउटपेशेंट देखभाल/इनपेशेंट देखभाल, विशेषीकृत मेडिकल (सुपर स्पेशियलिटी) देखभाल और अति विशेषीकृत मेडिकल देखभाल जो रोगी की आवश्यकता के अनुरूप होती है। आयूष के अंतर्गत आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होमियोपैथी मेडिकल सेवाएं भी प्रदान की जाती है।
मेडिकल सेवाएं एक विशाल आधारभूत व्यवस्था के जरिए प्रदान की जाती है। इस आधारभूत व्यवस्था में अस्पताल, डिस्पेंसरी, अनैक्सेज़ (उपभवन), स्पेशलिस्ट सेंटर, मॉडल डिस्पेंसरीज़-कम-डायग्नॉस्टिक सेंटर(एमडीडीसी), आईएमपी क्लीनिक्स और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों के साथ होने वाली व्यवस्था शामिल होते हैं। आउट-पेशेंट देखभाल की व्यवस्था ईएसआई डिस्पेंसरी, आईएमपी क्लीनिक्स और इम्प्लॉयर युटिलाइजेशन डिस्पेंसरीज (ईयूडी) के जरिए प्रदान की जाती है। इन-पेशेंट देखभाल ईएसआईसी/ईएसआईएस के जरिए और निजी अस्पतालों के सहयोग के जरिए प्रदान की जाती है। देशभर में ईएसआई योजना के तहत 1384 सर्विस डिस्पेंसरीज हैं और 1224 आईएमपी हैं। इन-पेशेंट देखभाल देशभर में फैले 151 ईएसआई अस्पतालों की श्रृंखला के जरिए प्रदान की जाती है। इस श्रृंखला में 36 प्रत्यक्ष रूप से संचालित ईएसआईसी अस्पताल और 115 राज्य ईएसआई अस्पताल शामिल हैं, जहां स्टेट गवर्न्मेंट हॉस्पिटल और अनैस्केज़ द्वारा प्रदान किए गए बेड्स को छोड़कर कुल लगभग 19000 बेड हैं। सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं का प्रावधान मुख्य रूप से देशभर के 1000 से अधिक निजी अस्पतालों के सहयोग से किया जाता है।
चिकित्सा देखभाल पर निर्धारित सीमा के भीतर 07:01 के अनुपात में ईएसआई निगम और राज्य सरकार के बीच व्यय साझा किया जाता है जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है। राज्यों में चिकित्सा सुविधा के स्तर को समुन्नत करने के लिए, चिकित्सा सुविधा योजना के संचालन के लिए राज्य सरकारों को भुगतान की जाने वाली धनराशि को 1200 रु. प्रति आईपी परिवार इकाई प्रति वर्ष से बढ़ाकर 1500 रु. कर दिया गया है 01.04.2012 से लागू। ईएसआईसी ने ईएसआई योजनाओं के तहत आने वाली चिकित्सा सुविधाओं में सुधार के लिए कार्य योजना तैयार किया है जिसमें अस्पतालों के आधुनिकीकरण का प्रावधान है जिसके अंतर्गत अस्पतालों में आपातकालीन और नैदानिक सुविधाओं को समुन्नयन करने, बीमारियों के प्रोफाइल के अनुसार विभागों का विकास करने, अपशिष्ट प्रबंधन, गहन चिकित्सीय देखभाल सेवाओं का प्रवाधान, शिकायतों के निबटारे की समुन्नत व्यवस्था, निरंतर शिक्षण कार्यक्रम, प्रयोगशालाओं के कंप्यूटरीकरण और समुन्नयन आदि की योजनाएं हैं। ईएसआईसी अस्पतालों और दवाखानों में इलाज के लिए आयुष व्यवस्था को चरण बद्ध तरीके से प्रोत्साहित और लोकप्रिय करने के लिए भी ईएसआईसी ने नए प्रयास किए हैं।
ईएसआईसी आईटी परियोजना पंचदीप वर्तमान में ई-गवर्नेंस के विशालतम परियोजनाओं में से एक है जो अभी क्रियान्वयन की प्रक्रिया से गुजर रही है। सभी ईएसआई संस्थानों को इस योजन अके तहत एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है ताकि आईपी और उनके परिवार के सदस्यों को ईएसआई लाभ कहीं भी और कभी भी उपलब्ध हो सके। “पहचान कार्ड” नामक दो स्मार्ट कार्ड जारी किए गए हैं, जिनमें से एक बीमाकृत व्यक्ति के लिए और दूसरा उसके परिवार के लिए है। साथ ही, सामाजिक सुरक्षा कवरेज को समुन्नत करने, बकाए की राशि के आकालन के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने और लाभार्थियों को बेहतर लाभ दिलाने के लिए ईएसआई एक्ट, 1948 में 01.06.2010 को संशोधन किय गया है। मौजूदा ईएसआईसी योगदान दरें हैं कर्मचारी- मजदूरी 1.75%, नियोक्ता- मजदूरी का 4.75%.
कवरेज का विस्तार
वर्तमान में, सामाजिक सुरक्षा नीति निर्माता और प्रशासक देश में सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए व्यापक परिचर्चा में लगे हैं। इस परिचर्चा में निजी प्रबंधन वाली सामाजिक योजनाओं के विरुद्ध सार्वजनिक प्रबंधन वाली सामाजिक योजनाओं की कुशलता के पक्ष में अनेक तर्क दिए गए हैं। इस मुद्दे पर ऐसा कोई मानक मॉडल नहीं है जिसे अपनाया जाए। भारतीय परिदृश्य में निजी प्रबंधन में चलाई जाने वाली योजनाओं को सार्वजनिक रूप से अनिवार्यतः चलाई जाने वाली योजनाओं के पूरक के रूप में मानना सबसे बढ़िया हल है। संपूर्ण कार्यबल तक पहुंचने के लिए केवल सार्वजनिक प्रबंधन वाली योजना ही उपयुक्त हो सकती है। सामाजिक सुरक्षा की उपलब्धता में कवरेज गैप को दूर करने की चुनौती से दो स्तरों पर निबटा जाना है। पहले स्तर में, कुशलता बढ़ाने के लिए सांस्थानिक व्यवस्थाओं का पुनर्निर्माण शामिल है। दूसरे स्तर पर, सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाने के लिए, खासकर असंगठित क्षेत्रों में, एक उपयुक्त वैधानिक एवं प्रशासनिक ढांचे का निर्माण किया जाना है। भारत में, 40 करोड़ कार्यबल में से अभी केवल 3.5 करोड़ कार्यबल की पहुंच वृद्धावस्था लाभ सुरक्षा के रूप में औपचारिक सामाजिक सुरक्षा तक है। इनमें शामिल हैं निजी क्षेत्रों के कामगार, सरकारी सेवक, सैनिक और राजकीय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के कर्मचारी। इस 3.5 करोड़ में से 2.6 करोड़ कामगार कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन के सदस्य हैं। भारत की मौजूदा सार्वजनिक प्रबंधन वाली व्यवस्था कमोबेश कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन द्वारा संचालित है। यह देखा जा सकता है कि पिछले 50 सालों के कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन के इतिहास में कभी कोई घोटाला या ऐसी किसी अनियमितता के मामले नहीं मिले हैं जहां निधि पर कभी कोई सवाल उठा हो या कभी उसपर कोई खतरा मंडराया हो। ईपीएफ का दूसरा महत्वपूर्ण योगदान जो अभी प्रस्तावित है वह यह कि इसे आवास उपलब्ध कराने के जीवन लाभ तक विस्तारित किया जाए। श्रमिक आवास योजना का लक्ष्य है ईपीएफ सदस्यों के लिए एक लागत प्रभावी आवास योजना उपलब्ध कराना। इसमें शामिल है प्रदाता के रूप में भूमिका निभाने में हुडको, हाउसिंग एजेंसियों, राज्य सरकारों, कर्मचारियों और ईपीएफ सदस्यों के बीच तालमेल की स्थपना। निवेश वित्त मंत्रालय द्वारा स्थापित पैटर्न के अनुसार अनुशंसित सुरक्षाओं और पोर्टफोलियो की ओर उन्मुख
| कार्यक्रम का नाम | कार्यक्रम के प्रकार | वित्त व्यवस्था | कवरेज |
|---|---|---|---|
| कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) | अनिवार्य | नियोक्ता: 1.67-3.67% कर्मचारी :10-12% सरकार: कोई नहीं | 20 कर्मचारियों के साथ फर्म |
| कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस | अनिवार्य | नियोक्ता: 8.33% कर्मचारी: कोई नहीं सरकार: 1.16% | 20 कर्मचारियों के साथ फर्म |
| कर्मचारियों जमा लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ईडीएलआई) | अनिवार्य | नियोक्ता: 0.5% कर्मचारी: कोई नहीं सरकार: कोई नहीं | 20 कर्मचारियों के साथ फर्म |
(इन कार्यक्रमों के तहत कार्यबल के कवरेज के विस्तार के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है)
| कार्यक्रम | कार्यक्रम के प्रकार | वित्त व्यवस्था | कवरेज |
|---|---|---|---|
| सिविल सेवा पेंशन योजना सरकारी भविष्य – निधि | अनिवार्य अनिवार्य | राज्य या केन्द्र सरकार कर्मचारी योगदान | राज्य और केन्द्र सरकार के स्तर के सिविल सेवक राज्य और केन्द्र सरकार के स्तर के सिविल सेवक |
| विशेष भविष्य निधि | अनिवार्य | नियोक्ता और कर्मचारी योगदान | विशेष क्षेत्र के कामगारों पर लागू: कोयला, खान, चाय बागान, जम्मू और कश्मीर, नाविक आदि |
| लोक भविष्य निधि | स्वैच्छिक | योगदान | सभी व्यक्ति आवेदन के पात्र हैं |
| वीआरएस योजना | स्वैच्छिक | योगदान | संबंधित प्रतिष्ठानों द्वारा निर्धारित कर्मचारी |
| निजी पेंशन | स्वैच्छिक | वार्षिकी प्रकार के उत्पादों का क्रय | सभी व्यक्ति |
| राज्य स्तरीय सामाजिक सहायता | सरकार द्वारा प्रायोजित सामाजिक सहायता | राज्य सरकार | राज्य और योजना के प्रकार के अनुसार बदलता रहता है |
| राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना | सरकार द्वारा प्रायोजित सामाजिक सहायता | केन्द्र सरकार | 65 साल की उम्र से ऊपर के गरीब व्यक्ति |